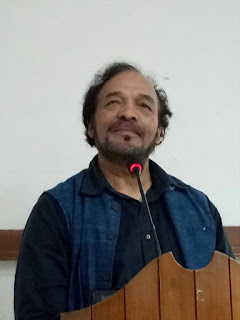सुसंस्कृत कौन और गँवार कौन?
साहित्य में ग्रामीण परिवेश की कई कहानियां प्रायः पढ़ने को मिल जाती
हैं। अपवादस्वरूप अधिकतर कहानियां गांव को पिछड़ा दर्शाती हैं। इन कहानियों में अगड़ा
शहर होता है। शहरी विकसित, समझदार, शिक्षित, संपन्न और दयालु। ग्रामीण गरीब, पिछड़े हुए, गंवार, अनपढ़, विपन्न और निष्ठुर। ये क्या बात हुई?
कहानियों में बाल जीवन की स्थिति तो और भी हास्यास्पद दर्शाई जाती है।
गांव में जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए कोई शहरी आता है और उसे हल कर देता
है। शहर के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में गांव में आते हैं और गांव के बच्चों को, गांव के बढ़े-बूढ़ों को शिक्षा और ज्ञान
देते हैं। यह भी गांव में रहने वाले बच्चों के सपने ही नहीं होते। उनके पास कोई दिशा
नहीं होती और वे मानों बेवकूफ हों।
साहित्यकारों को शहर में गरीबी नहीं दिखाई देती। गरीबी गांव में ही
होती है। गरीब होना जैसे गांव का पर्याय हो। गरीब बच्चे बुरी आदतों के शिकार हैं। उन्हें
कोई शऊर नहीं आता। शहरी बच्चे साल में तीज-त्योहारों में गरीब बच्चों का भला करने पर
उतारू दिखते हैं। गरीब बच्चों का बचपन मानों बेचारगी और दयनीयता बेचारगी से भरा पड़ा
होता है। उन्हें इतना बेचारा दिखाया जाता है जैसे गरीब बच्चे कभी हंसते ही न हों। खेलते
ही न हों। उनके पास मानों हंसने का भी अभाव हो। और तो और वे मन से कपटी होते हैं। वह
हमेशा चोरी-चकारी में लीन रहते हैं। मानो शहर में होने वाले अपराध भी गरीब ही करते
हैं। दीवाली, ईद
और यहां तक क्रिसमस के त्योहारों में सम्पन्न परिवार के बच्चे गरीब बच्चों की मदद करने
गांव में चले आते हैं। एहसान जताते भाव।
कहानियों में पशु-पक्षियों में ऐसे मानवीकरण दर्शाए जाते हैं जो हजम
ही नहीं होते। जंगल के जानवरों को शहरी जानवर आकर समझाता है। सिखाता है। हद है! जबकि
शायद यह अधिक सच जान पड़ता है कि अभाव में पले बच्चों में अधिकतर मानवीय संवेग दिखाई
पड़ते हैं। मूल्यों की उनमें कमी नहीं होती। वे अभाव में ही प्रभाव रखते हैं। सामूहिकता, सहयोग, भाईचारा और अपनत्व का भाव उनकी जरूरत
होती है। यही कारण है कि वह उनके रोजमर्रा के जीवन में अधिक दिखाई देते भी हैं।
कई बाल पत्रिकाओं में ऐसी कहानियों की भरमार है, जहां गर्मियों की छुट्टियों में शहर
से गांव आए बच्चे गांव के बच्चों को ज्ञान बघारते मिलते हैं। बहुत कम कहानियां ऐसी
हैं जो गरीब और उनके अभाव को मानवीय मूल्यों के साथ ईमानदारी से चित्रित करती हैं।
हालांकि मेरा ये मानना है कि एक धनाढ्य परिवार का बच्चा भी संवेदनशील हो सकता है। वह
दिल से बिना स्वार्थ के गरीब बच्चों की मदद भी कर सकता है। लेकिन आंकड़े, अनुभव और अनुपात के आधार पर अध्ययन
करें तो पाते हैं कि जो चित्रण गरीब, मासूम, असहाय, अल्पसंख्यक, दलित बच्चों की कहानियों में दिखाई
देता है उसमें सवर्ण-ठकुराहत भरा दंभ अधिक दिखाई पड़ता है।
बच्चों के नाम भी हमें पढ़ने को ऐसे मिलेंगे मानों नाम से ही पात्र का
भान अच्छे और खराब का हो जाए। हास्यास्पद बात यह भी है कि कहानियों में सभी पात्रों
के शानदार नाम होंगे। लेकिन काम वाली और उसके बच्चों के नाम नहीं होंगे। अखबार वाला, बर्तन वाली, दुकानदार, नाई, डाकिया, भिखारी, नौकर से अतिश्री कर ली जाती है। जैसे
इनके नाम ही नहीं होते। अब आप कहेंगे कि समाज में भी तो ये संज्ञाओं से पुकारे जाते
हैं। पर क्या हम ऐसा पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी रोजमर्रा के जीवन में इन कामगारों
को इनके नाम से नहीं पुकारते होंगे। होटलों में क्या कोई ऐसा ग्राहक न जाता होगा जो
वहां नौकरों को ऐ। ओ छोटू के अलावा इशारे से बुलाकर पहले नाम पूछ लेता होगा? ये भाव हमारी कहानियों का हिस्सा क्यों
नहीं होते?
कहानियों का आनंद लेते हुए कई बार बेमज़ा देने वाले प्रसंग मुझसे टकाराते
हैं। मसलन चोरी करना, दंगा
करना, शैतानी
करना गरीब बच्चे जन्म से लिखा कर लाते हैं। ज्ञान और अच्छी बातें जैसे अमीर बच्चों
की बपौती है। त्योहारों को हिन्दू और मुसलमान के त्योहार बताने वाली कहानियां अटी पड़ी
हैं। क्रिसमस से जुड़ी कहानियों में आपको अलबर्ट, जाॅन, स्टीया जैसे पात्र ही पढ़ने को मिलेंगे।
समरसता जगाता उदाहरण ढूंढें नहीं मिलता। ईद के प्रसंग से जुड़ी कहानियों में आपको शर्मा, पाण्डेय नहीं मिलेंगे। वहां आजम खान, तलीफ ही मिलेंगे। क्यों भाई? इन त्योहारों को आपने धर्म के आधार
पर काहे बांट लिया? ये
सब क्या है?
ऐसी कहानियों की भरमार है जो बालमन को छूती हैं लेकिन वहां जात-पांत, अमीर-गरीब के साथ प्रसंग खास सोच के
साथ रेखांकित होते हैं। गरीब बच्चों को भोंदू मानना कहां तक उचित है। जबकि शायद सचाई
यह है कि गरीब बच्चे और गांव के बच्चे मौसमों के बारे में, पेड़-पौधों के बारे में, तीज-त्योहारों के बारे में अधिक संवेदनशील
होते हैं। गरीब बच्चों के पास भले ही सुपर मार्केट जाने, माॅल जाने के लिए रुपए न हों। लेकिन
इसका मतलब यह नहीं कि वे रुपए का मोल न जानते हों। खरीदारी ही न करते हों। वे रेल, जहाज में न बैठे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे यात्रा
करते ही नहीं। यात्रा का आनंद लेना उनके शब्दकोश में है ही नहीं।
गरीबी का उपहास उड़ाने से बेहतर होगा कि गांव को हमारी कहानियों में
गहनता से आना चाहिए। गरीब की ज़िंदगी में जो मस्ती और उल्लास है। खुशी के क्षण हैं।
उनके बचपन में जो मस्ती है, उसे
हमारी कहानी में उभारा जाए।
बताता चलूं कि मेरा मंतव्य कतई शहरी और धनाढय बच्चों को बदमाश बताना
नहीं है। लेकिन सचाई यह भी है कि जिन बच्चों के पास कपड़े बदलने के कई विकल्प होते हैं।
तीन-तीन पेंसिलें, चार-चार
जोड़ी जूते एक साथ पहनने को होते हैं। उनकी थाली में कई तरह का भोजन होता है। ये एक
छोटा हिस्सा हैं। इस छोटे हिस्से के बनिस्पत वे बच्चे जिनके पास घर में पहनने के लिए
एक जोड़ी कपड़ा और बाजार आदि जाने के लिए एक जोड़ी ही दूसरा कपड़ा, लिखने के लिए एक मात्र छोटी हो चुकी
पेंसिल है। पहनने के लिए एक जोड़ी जूता ही है। ऐसा हिस्सा अधिक बच्चों का है। यह बड़ा
हिस्सा शायद रख-रखाव,सलीके
से चीज़ों को रखने और दूसरों की संभाल के भाव को अच्छे से महसूस करते हैं।
मेरा ऐसा सोचना सही है। यह मेरा कहना कतई नहीं है। लेकिन मित्रों जाने-अनजाने
में कई कहानियां जो हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वह मदद के भाव को स्थापित नहीं करतीं।
वह तो भीख और अहसान जताने के भाव को रेखांकित करती है। ऐसे भाव जो भीख देने जैसे लगते
हैं। दया जैसे भाव हावी हो जाते हैं। एक था रामू। रामू अमीर था। एक था श्यामू। वह बहुत
गरीब था। यह पहले ही स्थापित करते हुए मुझे जो कहानियां पढ़ने को मिलती है, मैं उनमें आनंद नहीं ले पाता। और यकीनन
उनमें अधिकतर कहानियां आदर्शवाद की भेंट चढ़ जाती हैं।
मनोहर चमोली ‘मनु’
कितना अच्छा हो कि कहानियों में ऐसे पात्र भी आएं जो गरीबों की जरूरतमंदों
की मदद करते हुए पाठकों को तो दिखाई दें लेकिन जिनकी मदद की जा रही है उन्हें पता ही
न चले। कहानियों में कई बार ऐसा लगता है कि मदद करना, सहयोग करना, किसी के काम आना जलसा बुलाकर ही किया
जा सकता है। तब यह दूसरा ही मामला हो जाता है।
अनपढ़ कौन है? वही
तो जो मात्र लिखी हुई इबारत को पढ़ नहीं पाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बेवकूह
है। अज्ञानी है। नासमझ है। वहीं गंवार कौन? जो गांव में रहता है वह गंवार हुआ।
लेकिन गंवार का मायने यह मान लिए गए हैं जो जाहिल है वही गंवार है। जो भुस्स है वह
गंवार है। शहर में रहने वाला शहरी और गांव में रहने वाला गंवार या गंवई। तो किसी को
गंवार कहने से पहले हमें समझ लेना होगा कि हम गंवार किन संदर्भों में कह रहे हैं। एक
गांव का आदमी शहर में आकर भी रह सकता है। एक शहरी शेष जीवन गांव में भी बिता सकता है।
बहरहाल, आज
भी हमारे समाज में ऐसे कई हैं जो गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों की खूब मदद करते हैं।
लेकिन गुप्त रूप से। वह उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। हमारी कहानियों में भी ये मानवीय
मूल्य और संवेग आएं। जरूर आए लेकिन दूसरों पर अहसान जताने के लिए न आए। ऐसे आएं जैसे
हवा का बहना जरूरी है। सूरज का रोशनी बिखेरना जरूरी है। साहित्यकारों को समझना होगा
कि पाठक भी सुसंस्कृत हो सकते हैं और साहित्यकार भी। पाठक भी साहित्यकार के साहित्य
की समझ रख सकते हैं और नहीं भी। लेकिन पाठकों को कमतर आंकना ठीक नहीं। और हां, यहां तक पढ़ा है तो आपका कुछ कहना भी
जरूरी है। कहेंगे न? कुछ
तो कहेंगे। ॰॰॰
-मनोहर चमोली ‘मनु’,
भितांई,पोस्ट-23,निकट डिप्टी धारा, पौड़ी 246001
उत्तराखण्ड।
सम्पर्कः 09412158688
व्हाट्स एप-07579111144